
“जब इतिहास दिल्ली दंगों को देखेगा तो यह बात जरूर चुभेगी कि जाँच एजेंसी ने सही तरीक़े से और आधुनिक वैज्ञानिक तरीक़ों का इस्तेमाल करके जाँच नहीं की. यह विफलता लोकतंत्र के पहरेदारों को निश्चित रूप से परेशान करेगी.”
ये कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद यादव के शब्द हैं.
इन्होंने अपने दो फ़ैसलों में ये टिप्पणी की. उन्होंने यह भी कहा था कि इन दो मामलों में जाँच बहुत ख़राब तरीक़े से हुई है और ‘जाँच एजेंसी ने बस अदालत की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश की है.’
पुलिस के कामकाज पर यह एक तल्ख़ टिप्पणी मानी जा सकती है.
पिछले पाँच सालों में ऐसे कई मामले हैं जिसमें कोर्ट ने पुलिस की बहुत आलोचना की है. जैसे, कोर्ट ने किसी मामले में कहा कि ‘जाँच सही से नहीं की गई’ या ‘अभियुक्त को ग़लत तरीक़े से फँसाया गया है’ तो किसी मामले में कहा, ‘पहले से तय धारणा के आधार पर चार्जशीट दायर की गई है.’
साल 2020 के फरवरी में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए आँकड़ों के मुताबिक़ दंगों में 53 जानें गई थीं. इनमें 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे. इनके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए. करोड़ों की संपत्ति का नुक़सान हुआ.
पुलिस ने दंगों से जुड़े 758 एफ़आईआर दर्ज़ किए. ख़बरों के मुताबिक, पुलिस ने दो हज़ार से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया था.
लेकिन बड़ा सवाल है, पाँच साल बाद कितनों को इंसाफ़ मिला?
पिछले 2 महीनों में बीबीसी हिंदी ने इन सारी एफ़आईआर की मौजूदा स्थिति देखी. कोर्ट के फैसलों का अध्ययन किया.
हमने पाया कि बहुत कम मुकदमों में अभियुक्तों को दोषी पाया जा रहा है. यही नहीं, 80 फ़ीसदी से ज़्यादा केसों में अभियुक्त या तो बरी हो रहे हैं या ‘डिस्चार्ज’.
डिस्चार्ज यानी वो मामले जिसमें पुलिस की चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट को आरोप तय कर करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिखे.
120 से ज़्यादा फ़ैसलों में 20 केस ऐसे मिले जिसमें लोग दोषी पाए गए हैं. इसमें भी 12 मामले ऐसे हैं जिनमें अभियुक्तों ने अपना गुनाह क़बूल कर लिया था.
यह जानने के लिए कि आख़िर इतने कम मामलों में लोग दोषी क्यों पाए जा रहे हैं, बीबीसी हिंदी ने 126 फ़ैसलों का भी विश्लेषण किया.
हमने इस बारे में दिल्ली पुलिस से मिलकर बात करने की कोशिश की.
उनको ई-मेल के ज़रिए कई बार सवाल भी भेजे पर हमें जवाब नहीं मिला. हालाँकि, दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल एक जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हर केस की जाँच ‘निष्पक्ष और सही तरीक़े से हुई है.’
758 एफ़आईआर की ‘स्टेटस’ जानने के लिए बीबीसी हिंदी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी पाने के लिए आवेदन किया. हमें आरटीआई से 62 केस की सूचना मिली. ये सारे केस हत्या से जुड़े हैं.
अप्रैल 2024 में पुलिस ने कोर्ट के सामने एक ‘स्टेटस रिपोर्ट’ दाख़िल की थी. इसमें उन्होंने इन सभी केस में क्या चल रहा है, यह बताया था.
पुलिस ने बताया था कि क़रीब 38% (289) केसों में तहक़ीक़ात चल रही थी. क़रीब 39% (296) में तहक़ीक़ात पूरी होने के बाद कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और बचे 23% (173) केस में या तो फ़ैसला आ गया था या उन्हें खारिज कर दिया गया था.
758 एफ़आईआर में से 62 मामले हत्या से जुड़े थे. ये मामले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपे गए थे. हमारी आरटीआई आवेदन के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनमें से अब तक सिर्फ़ एक केस में अपराधी ठहराया गया है. चार मामलों में लोग बरी हुए. वहीं, 39 में मुकदमा जारी है और 15 में जाँच.
बीते दिसंबर ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 वर्षीय मोनिश उर्फ़ मोसिन की ग़ैर इरादतन हत्या के लिए पाँच लोगों को सात साल की सज़ा दी थी.
वहीं, एक केस दिल्ली दंगों की साज़िश से जुड़ा है. इसमें 18 लोगों पर गैरक़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए की धाराएँ लगाई गई हैं. इसे आतंकवाद से जुड़ा क़ानून भी माना जाता है. इस मामले में अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है.
जिन केस में फ़ैसले आए हैं, उनमें अब तक 80% से ज़्यादा केस में अभियुक्त बरी या डिस्चार्ज हो गए हैं.
पुलिस के डेटा के मुताबिक, अप्रैल 2024 तक 19 मामलों में लोगों को दोषी पाया गया. वहीं, 76 केस ऐसे थे जिनमें ट्रायल के बाद लोगों को बरी कर दिया गया. 16 केस ऐसे थे जिसमें अभियुक्त ‘डिस्चार्ज’ हो गए. यानी पुलिस की चार्जशीट दायर होने के बाद अदालत को इन केसों में ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले.
हमने इस साल जनवरी में सभी 758 मामलों की मौजूदा स्थिति कड़कड़डूमा कोर्ट की वेबसाइट पर देखी. हमने पाया कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच और 18 केस में लोग बरी हुए और एक केस में अभियुक्तों को दोषी पाया गया.
पुलिस की अप्रैल 2024 तक दी गई जानकारी और बीबीसी हिंदी के विश्लेषण को मिला कर देखें तो अबतक 94 मामलों में लोगों को बरी किया गया, 16 में डिस्चार्ज और सिर्फ़ 20 में दोषी पाया गया.
बीबीसी हिंदी ने 126 फ़ैसलों का भी विश्लेषण किया. इसमें 92 में लोग बरी हुए. 14 में डिस्चार्ज और 20 में दोषी पाए गए.
पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में दिए गए दो डिस्चार्ज और दो बरी होने वाले मामलों से जुड़े फ़ैसले हमें कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं मिले.
20 मुकदमों में 12 ऐसे थे जिनमें अभियुक्तों ने अपना गुनाह क़बूल कर लिया था.
जिन्होंने अपने गुनाह क़बूल किए, उनके बारे में कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जितना समय जेल में बिताया है, उतना पर्याप्त है.
जैसे, छह केस दो अभियुक्तों के ख़िलाफ़ थे. उन पर दंगा, आगज़नी और चोरी करने के आरोप थे. इसमें सात साल तक सज़ा हो सकती है.
अदालत ने उन्हें 76 दिनों में रिहा कर दिया. वहीं, दो केस में अदालत ने दो अभियुक्तों को 97 और 36 दिन की सज़ा पर्याप्त बताई. बाक़ी के केस जिसमें अभियुक्तों ने गुनाह क़बूल किया, उनमें क़रीब ढाई साल की सज़ा दी गई.
ऐसे केस जिनमें कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया, उसमें तीन से लेकर सात साल तक की सज़ा दी गई.
हमने कोर्ट के उन 106 फ़ैसलों का भी विश्लेषण किया जिसमें अभियुक्तों को निर्दोष पाया गया. इस विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष निकले हैं.
अभियुक्तों के बरी होने के दो कारण मुख्य थे. पहला कारण था, क़रीब आधे यानी 49 केस में गवाह अपने पहले के बयान से पलट गए. यानी गवाही देते समय उन्होंने पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत केस का समर्थन नहीं किया.
दूसरा कारण था, क़रीब 60% यानी 66 केस ऐसे थे जिनमें पुलिस वाले ही गवाह थे. कई कारणों से कोर्ट ने उनके बयान को विश्वसनीय नहीं माना.

इनमें कुछ केस में पुलिस वालों के बयानों में परस्पर विरोध था. कोर्ट ने आशंका जताई कि वे सच नहीं बोल रहे हैं या यह कहा कि उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता.
कुछ ऐसे केस भी थे, जिसमें पुलिस ने अभियुक्तों की ‘पहचान’ काफ़ी दिनों बाद की थी. कोर्ट ने उनके बयान पर सवाल खड़े किए. कोर्ट का सवाल था कि जब पुलिस वाले रोज़ थाने जा रहे थे और उन्हें पता था कि दंगों से जुड़े केस की तहक़ीक़ात चल रही तो अभियुक्तों को पहचानने में देरी होने से उनके बयान पर संदेह पैदा होता है.
कुछ केस ऐसे थे जिसमें ड्यूटी शीट के मुताबिक गवाही देने पुलिस वालों की तैनाती किसी और इलाक़े में थी और वे गवाही किसी और इलाक़े के बारे में दे रहे थे. ऐसे में कोर्ट ने उनके बयान को विश्वसनीय नहीं माना.
कम से कम नौ केस ऐसे हैं जिसमें एक पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि वे अपनी याददाश्त खो रहे हैं. इनमें से आठ केस में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया और एक में दोषी पाया गया.
अपनी पहली गवाही में वे अभियुक्तों की पहचान नहीं कर पाए थे पर दूसरे केस में उन्होंने उन्हीं अभियुक्तों की पहचान कर ली. जब उनकी इस पहचान पर सवाल खड़े किए गए तो उन्होंने कहा कि उनकी याददाश्त जा रही है. वे इसके लिए दवाई भी ले रहे हैं. इसलिए वह पहले मामले में पहचान नहीं कर पाए थे.
बाकी केस में भी एएसआई ने जब उन्हीं अभियुक्तों की पहचान की तो ये बात हर केस में उठी कि वे पहले उनकी पहचान नहीं कर पाए थे.
कोर्ट ने शुरू के कुछ मामलों में कहा कि वे अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग दावे कर रहे हैं, इसलिए उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता. उसके बाद, उन्होंने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कोर्ट में जामा किया. डॉक्टर को भी कोर्ट में पेश किया. डॉक्टर ने कहा कि एएसआई को चक्कर आने की शिकायत है. इससे दिमाग़ में भी असर पड़ता है.
इसके बाद आख़िरी के कुछ मामलों में कोर्ट ने कहा कि उनके पहले के बयानों से आगे आने वाले केस पर फ़र्क़ नहीं पड़ना चाहिए.
अभियुक्तों के बरी होने के कुछ और कारण भी थे. क़रीब 15% (16) मामलों में पुलिस ने अपनी तहक़ीक़ात में वीडियो साक्ष्य पर भरोसा किया. ये साक्ष्य या तो कोर्ट में पेश नहीं हुए या उनकी कोर्ट में पुष्टि नहीं हो पाई. इसलिए कोर्ट ने उस पर भरोसा नहीं किया.
कुछ ऐसे भी मामले थे जिसमें कोई गवाह या सबूत नहीं थे. कुछ ऐसे मामले भी थे, जहाँ एक से ज़्यादा कारणों से लोग बरी हो गए. जैसे, गवाहों का पलटना, पुलिस के बयान का विश्वसनीय न होना और वीडियो सबूत ठीक से पेश न करना.
हमारे विश्लेषण में एक और बात उभर कर आई कि कई केस में कोर्ट ने पुलिस के तहक़ीक़ात की कड़ी आलोचना की. बरी और डिस्चार्ज होने वाले 50 से ज़्यादा मामलों में कोर्ट ने पुलिस के तहक़ीक़ात या उनके बयानों पर कई सवाल खड़े किए.
इनमें कुछ फ़ैसलों में कोर्ट ने कहा कि ‘चार्जशीट बिना जाँच के दायर की गई है.’ ‘गवाहों के बयान झूठे लग रहे हैं.’ ‘किसी निर्धारित-धारणा के आधार पर लोगों को अभियुक्त बनाया गया हैं.’ एक फ़ैसले में जज ने कहा, “नया बयान इसलिए रिकॉर्ड किया गया कि प्रॉसिक्यूशन के केस में जो कमी है, उसे छिपाया जा सके. अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट को उचित बताया जा सके.”
एक ऐसा भी केस था जिसमें कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की है. आधा वीडियो कोर्ट में पेश किया ताकि ग़लत इंसान को फँसाया जा सके.
एक फ़ैसले में अभियुक्तों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जाँच में बहुत कमियाँ थीं. जज ने कहा, “इस बात की संभावना है कि गवाह के रूप में दो पुलिस वालों का इस्तेमाल बस इसलिए किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि केस हल हो गया है.”
कुछ मामलों में कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी शिकायतों की एक साथ जाँच की गई, जो सही नहीं थी. इनमें से कुछ केस में कोर्ट ने कहा कि पुलिस को शिकायतों की जाँच दोबारा से करनी होगी.
यही नहीं, कम से कम दो मामले में कोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया. कम से कम दो मामले ऐसे भी थे जहाँ कोर्ट ने सीनियर अफ़सर को जाँच अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा.
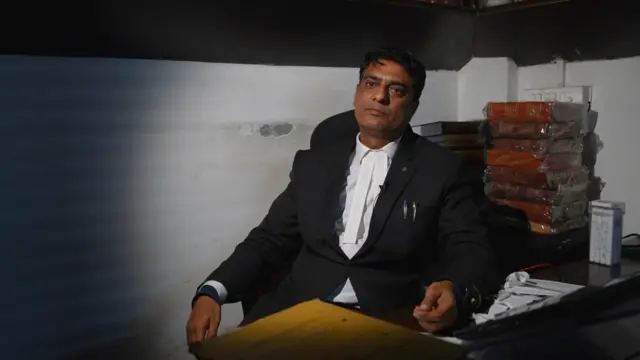
हमने दो वकीलों से भी बात की जो दंगों के कई केस से जुड़े हैं.
अब्दुल ग़फ़्फ़ार दिल्ली दंगों के 100 से ज़्यादा केस से जुड़े हैं. वे कहते हैं, “आम तौर पर पुलिस अफ़सर के पास केस कम होते हैं तो उन पर भार कम होता है. जाँच अच्छे तरीक़े से होती है. दंगों के केस में क़रीब 80-90% केस में जाँच उस स्तर की नहीं हो पाई.”

रक्षपाल सिंह भी वकील हैं. वे क़रीब 90 केस से जुड़े हैं. वे कहते है कि जाँच में कमियाँ थीं पर “यह भी देखते की ज़रूरत है कि दंगों के ठीक बाद कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया. इतने सारे केस की जाँच करने के लिए पुलिस के पास संसाधन कम थे.”
दोनों ने इस चीज़ का ज़िक्र भी किया की कई गवाह भी अपने बयान से पलट रहे हैं. इसकी वजह से भी केस साबित नहीं हो रहे.
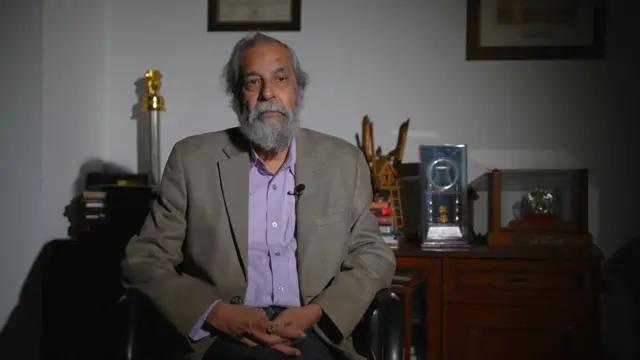
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर ने कहा, “प्रॉसिक्यूशन और पुलिस को बैठ कर सोचना चाहिए कि उन्होंने पाँच सालों में क्या हासिल किया.”
उन्होंने यह भी कहा कि किसी को जेल में डालने पर पुलिस और प्रॉसिक्यूशन की भी जवाबदेही होनी चाहिए. वे कहते हैं, “लोग सालों जेल में रहते हैं और फिर बेल पर (या बरी होकर) बाहर आते हैं और कुछ नहीं होता. जो उन्हें जेल में डालते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं होता.”
उनका कहना है कि अगर ये पाया जाए कि जेल में डालना ग़ैर-क़ानूनी था या जेल में डालने की ज़रूरत नहीं थी, ‘तो पुलिस और प्रॉसिक्यूशन की जवाबदेही भी तय करना ज़रूरी है.’